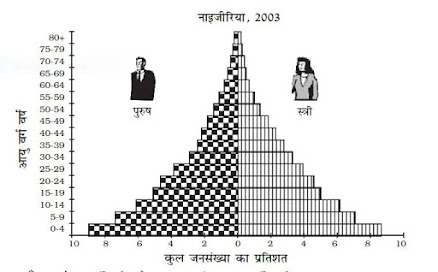मानव बस्ती - मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित घरों का संगठित समूह जिनमे मनुष्य रहते है मानव बस्ती कहलाती है आधारभूत कार्यों के आधार पर मानव बस्तियां दो प्रकार की होती हैं।
1. ग्रामीण बस्तियाँ 2. नगरीय बस्तियाँ
1. ग्रामीण बस्तियाँ - ऐसी बस्तियाँ जिनमें निवास करने वाले लोग कृषि या प्राथमिक क्रियाकलापो में संलग्न रहते हैं ग्रामीण बस्तियाँ (गाँव) कहलाती हैं
ग्रामीण बस्तियाँ अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती हैं अतः ग्रामीण लोगों का भूमि से निकट संबंध होता है
2. नगरीय बस्तियाँ - ऐसी बस्तियाँ जिनमें निवास करने वाले अधिकांश लोग द्वितीयक या तृतीयक व्यवसाय में संलग्न रहते हैं नगरीय बस्तियाँ कहलाती हैं नगरीय बस्तियाँ अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति द्वितीयक या तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से करती हैं
ग्रामीण बस्तियों के प्रकार
आकृति के आधार पर बस्तियों को मुख्यतया निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
1. संहत बस्ती: इन बस्तियां में मकान पास-पास पाये जाते है इस तरह की बस्तयों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। इन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्ति मिल-जुलकर रहते हैं तथा इनमें से अधिकांश व्यक्तियों के व्यवसाय समान होते हैं।
2. प्रकीर्ण बस्ती: इन बस्तियों में मकान दूर-दूर होते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा-स्थल अथवा बाजार इन बस्तियों को एक साथ बाँधता है।
ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक
1. जल आपूर्ति - साधरणतया ग्रामीण बस्तियाँ नदियाँ, झीलें एवं झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती हैं, जहाँ जल आसानी से उपलब्ध् हो जाता है। कभी-कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्यथा असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों अथवा नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करते हैं।
2. भूमि - मनुष्य बसने के लिए उस स्थान का चयन करता है जहाँ की भूमि खेती के लिए उपयुक्त व उपजाऊ हो। किसी भी क्षेत्र में प्रारम्भिक अधिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में ही बसते थे। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्र में बस्तियाँ नहीं बसाई जाती हैं जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियाँ बसाते हैं जो कि उन्हें नम चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं।
3. उच्च भूमि के क्षेत्र - मानव ने अपने अधिवास हेतु ऊँचे क्षेत्रों को इसलिए चुना कि वहाँ पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके एवं मकान व जीवन सुरक्षित रह सके। नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियाँ नदी वेदिकाओं एवं तटबंधें पर बसाई जाती हैं क्योंकि ये भाग ‘शुष्क बिंदु’ होते हैं। उष्ण कटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं जिससे कि बाढ़ एवं कीडे़-मकोड़ों से बचा जा सके।
4. गृह निर्माण सामग्री - मनुष्य अपनी बस्तियाँ वहाँ बसाता है जहाँ आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं। प्राचीन गाँवों को वनों को काटकर बनाया गया था, क्योंकि वहाँ लकड़ी बहुतायत में थी। चीन के लोयस क्षेत्र में वहाँ के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे एवं अफ्रीका के सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनते थे जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो हिम खंडों से अपने घर (इग्लू) का निर्माण करते हैं।
5. सुरक्षा- राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या उपद्रव होने की स्थिति में गाँवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। नाइजीरिया में खडे़ इंसेलबर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। भारत में अधिकतर दुर्ग उँचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर स्थित हैं।
नियोजित बस्तियाँ
सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर एक कुशल योजना के माध्यम से सभी प्रकार कीं सुविधाएँ उपलब्ध कराकर विकसित की गई बस्ती नियोजित बस्ती कहलाती है सरकार द्वारा अधिगृहित की गई भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएँ जैसे आवास, पानी तथा अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध कराकर नियोजित बस्तियों को विकसित किया जाता हैं। इथोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना एवं भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास इसके अच्छे उदाहरण हैं।
ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप
ग्रामीण बस्तियों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप कहा जाता है ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है:
(i) विन्यास के आधार पर:
1. मैदानी ग्राम 2. पठारी ग्राम 3. तटीय ग्राम 4.वन ग्राम 5.मरुस्थलीय ग्राम
(ii) कार्य के आधार पर:
1.कृषि ग्राम 2.मछुवारों के ग्राम 3. लकड़हारों के ग्राम 4.पशुपालक
(iii) बस्तियों की आकृति के आधार पर:
(क) रैखिक प्रतिरूप: जब मकान या आवास सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी या सागर तट पर पंक्तिबद्ध रूप से स्थित होते हैं तो ऐसे प्रतिरूप को रेखीय प्रतिरूप कहते हैं।
(ख) आयताकार प्रतिरूप: जब दो सड़के एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो उनके मिलन स्थल पर दोनों सड़कों के किनारे लम्बवत गलियों का निर्माण होता है तो आयताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है।
(ग) वृत्ताकार प्रतिरूप: किसी झील, तालाब या चौपाल के चारों ओर मकान बनाने से निर्मित अधिवास वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाता है
(घ) तारा प्रतिरूप : जब अरीय प्रतिरूप में बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे मकान बन जाते हैं तो तारा प्रतिरूप का निर्माण होता है: जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं आरै उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं वहाँ तारे के आकार की बस्तियाँ विकसित होती हैं।
(ड) ‘टी’ आकार, ‘वाई’ आकार, क्रॉस आकार: टी के आकार की बस्तियाँ सड़क के तिराहे पर विकसित होती हैं। जबकि वाई आकार की बस्तियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। क्रॉस आकार की बस्तियाँ चौराहों पर प्रारंभ होती हैं जहाँ चौराहे से चारों दिशा में बसाव आरंभ हो जाता है।
(च) दोहरे ग्राम: नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है।
ग्रामीण बस्तियों की समस्याएँ
1. आवागमन के साधनों का अभाव- कच्ची सड़क एवं आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यहाँ की प्रमुख समस्या है। वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों का संपर्क आसपास के क्षेत्र से कट जाता है जिससे आपतकालीन सेवाएँ प्रदान करने में भी गंभीर कठिनाइयाँ उपलब्ध् हो जाती है।
2. जल की अपर्याप्त आपूर्ति - विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेय जल हेतु लंबी दूरियाँ तय करनी पड़ती हैं। जल जनित बीमारियाँ जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्या है। दक्षिणी एशिया के देश प्रायः बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। सिंचाई सुविधएँ कम होने से कृषि कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है।
3. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का अभाव- विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करना ग्रामीण बस्तियों की सबसे बड़ी समस्या है। यह समस्या उस समय और विकट हो जाती है जब ग्रामीणीकरण उचित प्रकार से नहीं हुआ है और विशाल क्षेत्र में मकान दूर तक विकसित होते हैं।
4. शौचघर एवं कूड़ा-कचरा निस्तारण का अभाव- ग्रामीण बस्तियों में शौचघर एवं कूड़ा-कचरा निस्तारण की सुविधाएँ नगण्य हैं। जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ रहती हैं।
5. जीवन की निम्नतर दशाएं - ग्रामीण बस्तियों में मकान घटिया स्तर की निर्माण सामग्री से बने होते है उन्हे भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय काफी नुकसान पहुँचता है मकानों में उपयुक्त संवातन नहीं होता है। एक ही मकान में मनुष्यों के साथ पशु भी रहते हैं।
6. रोजगार के अवसरों का अभाव - ग्रामीण बस्तियों में रोजगार के सिमित साधन होते है यहाँ मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है
नगरीय बस्तियाँ
लंदन को विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती होने का गौरव प्राप्त है 1982 में विश्व में करीब 175 नगर थे। वर्तमान समय में 48 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है
नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण
नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण सामान्य आधार जनसंख्या का आकार, मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय, प्रशासकीय ढाँचा एवं स्थिति है।
1. जनसंख्या का आकार
नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटाइना एवं पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, भारत में 5000 एवं जापान में 30,000 व्यक्ति हैं। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर होना चाहिए विभिन्न देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व वाला मापदंड उसी के अनुरूप बढ़ा या घटा दिया जाता है। डेनमार्वफ, स्वीडन एवं फिनलैंड में 250 व्यक्तियों की जनसख्ंया वाले सभी क्षत्र नगरीय क्षत्र कहलाते है
2. व्यावसायिक संरचना
जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियाँ निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड माना जाता है। इसी प्रकार इटली में उस बस्ती को नगरीय कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50 प्रतिशत गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। भारत में यह मापदंड 75 प्रतिशत का रखा गया है।
3. प्रशासन
कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने हेतु प्रशासनिक ढाँचे को मापदंड माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहाँ नगरपालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति है। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के देश ब्राजील एवं बोलीविया में जनसंख्या आकार का ध्यान नहीं रखते हुए किसी भी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केद्र माना जाता है।
4. स्थिति
नगरीय केन्द्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है।सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह हो जहाँ इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिले। खनिज नगरों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिजों का पाया जाना आवश्यक है औद्योगिक नगरों के लिए स्थानीय शक्ति के साधन एवं कच्चा माल, पर्यटन केंद्र के लिए आकर्षक दृश्य या सामुद्रिक तट, औषधीय जल वाला झरना या कोई ऐतिहासिक अवशेष तथा पत्तन के लिए पोताश्रय का होना।
उप नगरीकरण
यह नगरीकरण की एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मानव बड़े शहर के सघन बसे क्षेत्रों में स्थित आवासों छोड़कर शहर से बाहर एक ऐसे खुले व स्वच्छ बातावरण में अपना आवास बनाकर रहने लगता है जहाँ रहन-सहन को उत्तम सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। इस प्रक्रिया से बड़े शहरों के निकट ऐसे उपनगर विकसित हो जाते हैं, जहाँ प्रतिदन हजारों व्यक्ति बड़े शहरों में स्थित कार्य स्थलों पर आते-जाते हैं।
1991 की भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया है। ‘सभी स्थान जहाँ नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति (नोटीफाइड टाउन एरिया कमेटी) हो एवं कम से कम 5000 व्यक्ति वहाँ निवास करते हों, 75 प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हों व जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसे स्थान या क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहते है
नगरीकरण - नगरीकरण से तात्पर्य एक देश की नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि से है। नगरीकरण का प्रमुख कारण ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास है।
नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण
विशेषीकृत प्रकार्यों के आधार पर नगरों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है
1. प्रशासनिक नगर
राष्ट्र की राजधनियाँ जहाँ पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। जैसे नयी दिल्ली, केनबेरा, बीजिंग, अदीस अबाबा, वाशिंगटन डी.सी. एवं लंदन इत्यादि प्रशासनिक नगर हैं।
2. व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर
ऐसे नगर जिसके द्वारा किये जाने वाले केन्द्रीय कार्यों में व्यापार एवं व्यावसाय की प्रधानता होती है, व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर कहलाते हैं। जसे कृषि बाजार कस्बे जैसे विनिपेग एवं कंसास, बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर जैसे फ्रेंकफर्ट एवं एमसटर्डम, विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर एवं सेंट लूइस एवं परिवहन केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद एवं आगरा आदि
3. धार्मिक और सांस्कृतिक नगर
धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व वाले नगर सांस्कृतिक नगर कहलाते है जैसे जैरूसलम, मक्का, जगन्नाथ पुरी एवं बनारस
इनके अतिरिक्त अन्य नगरों में स्वास्थ्य एवं मनोरंजन नगर (मियामी एवं पणजी), औद्योगिक नगर (पिट्सबर्ग एवं जमशेदपुर), खनन नगर (ब्रोकन हिल एवं धनबाद) एवं परिवहन नगर (सिंगापुर एवं मुगलसराय) आदि सम्मिलित हैं।
आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण
एक नगरीय बस्ती रेखीय, वर्गाकार, तारा के आकार या अर्ध चंद्राकार (चापाकार) हो सकती है। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति, वास्तुकला एवं भवनों की शैली वहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाये गए हैं जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक है तथा उनकी आकृति अनियमित है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ एवं केनबरा नियोजित नगर हैं जबकि भारत में छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर की ओर बडे़ नगरीय फैलाव में गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए हैं।
अदीस अबाबा (नवीन पुष्प)
अदीस अबाबा इथोपिया की राजधनी है यह इथोपिया के मध्य में स्थित है जैसा कि इसके नाम से विदित होता है (अदीस-नया, अबाबा-पुष्प) एक नया नगर है जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है राजकीय मुख्यालय प्याज्जा, अरात एवं आमिस्ट किलो से चारों ओर सड़कें जाती हैं। उत्तर में काहिरा एवं दक्षिण में जोहंसबर्ग के बीच मरकाटो में सबसे बड़ा बाजार है। अदीस अबाबा जहाँ एक बहु संकाय विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं कई अच्छे स्कूल होने की वजह से शिक्षा का भी एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है। जिबूती अदीस अबाबा रेलमार्ग का अंतिम स्टेशन है। बोले हवाई अड्डा एक नया हवाई अड्डा है।
केनबेरा
अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर बरली ग्रिफिन ने 1912 में आस्ट्रेलिया की राजधनी के लिए इस नगर की योजना बनाई। भू-दृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस उद्यान नगर की कल्पना की थी। इसमें पाँच मुख्य केंद्र थे, प्रत्येक के अलग-अलग कार्य थे। पिछले कुछ दशकों में कई उपनगर इसके समीप बन गए हैं यहाँ कई उद्यान तथा पार्क हैं।
नगरीय बस्तियों के प्रकार
नगरीय बस्ती अपने आकार, उपलब्ध् सुविधओं एवं उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधर पर कई नामों से पुकारी जाती हैं जैसे नगर, शहर, मिलियन सिटी, सन्नगर, विश्वनगरी।
1. नगर - एक लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास नगर कहलाते हैं
2. शहर - शहर नगरों से बडे़ होते हैं यह अग्रणी नगर होता है। लेविस ममफोर्ड के शब्दों में, ‘वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप हैं।’
3. मिलियन सिटी - जिन नगरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। जैसे – लंदन, पेरिस, न्यूयार्क आदि विश्व में 2005 तक 438 व 2016 तक 512 मिलियन सिटी थे
4. सन्नगर - सन्नगर शब्द सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गिडिज(1915) ने किया था। मूलतः अलग-अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र बन जाता है। जिसे सन्नगर कहते हैं जैसे लंदन, टोक्यो, शिकांगो, दिल्ली-गुडगांव
5. विश्वनगरी - विश्वनगरी यूनानी शब्द ‘मेगालोपोलिस’ से बना है जिसका अर्थ होता है ‘विशाल नगर’। इसका प्रयोग 1957 में जीन गोटमेन ने किया। एक ऐसा बड़ा महानगर प्रदेश जिसमें कई सन्नगरों का समूह मिलाता है। विश्वनगरी कहलाता है इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है विश्वनगरी का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है।
6. मेगासिटी - ऐसे महानगर जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर एक करोड़ से अधिक हो। मेगासिटी कहलाते है विश्वि में वर्तमान में 25 मेगासिटी है सबसे पहला मेगासिटी न्यूयार्क है इसके अलावा टोक्यो, मुंबई, दिल्ली, ओसाका, कोलकाता, काहिरा, ढाका अन्य मेगासिटी है
नगरीय बस्तियों की समस्याएँ
रोजगार के अवसर एवं नागरिक सुविधाओं के लिए मानव शहरों की ओर आता है। परंतु विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित हैं अतः आने वाले व्यक्ति अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा कर देते हैं विकासशील देशों के आधुनिक शहरों मे आवासों कमी, लम्बवत विस्तार (बहुमंजिला मकान) तथा गन्दी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख विशेषताएँ हैं। अनेक शहरों में जनसंख्या का बढ़ता भाग निम्न स्तरीय आवासों जैसे गंदी बस्तियों, अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं।
1. आर्थिक समस्याएँ
विश्व के विकासशील देशों के ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यह विशाल प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में अकुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों, की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देती है
2. सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएँ
विकासशील देशों के शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त हैं। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण नगरों की अधिकतर जनसंख्या की आधरभूत आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती हैं। उपलब्ध् स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएँ गरीब नगरवासियों की पँहुच से बाहर रहती हैं। बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण इन नगरों में जनसंख्या का लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है।
3. पर्यावरण संबंधी समस्याएँ
विकासशील देशों में रहने वाली विशाल नगरीय जनसंख्या घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। एक अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वास्थ्यकर दशाएँ पैदा करती हैं। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को सामान्य मल-व्यवस्था में डाल दिया जाता है या बिना किसी शोधन के अनिश्चित स्थानों में डाल दिया जाता है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंकरीट ढाँचे बनाए जाते हैं जो नगरों में ‘उष्म द्वीप’ बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं।
स्वस्थ शहर
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर में निम्न सुविधएँ अवश्य होनी चाहिए:
1. ‘स्वच्छ’ एवं ‘सुरक्षित’ वातावरण
2. सभी निवासियों की आधरभूत आवश्यकताओं की पूर्ति
3. स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी
4. सभी के लिए आसानी से उपलब्ध् स्वास्थ्य सुविधएँ
नगरीय रणनीति की योजना
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ‘नगर रणनीति’ में निम्न प्राथमिकताएँ बताई हैंः
1.नगरीय निर्धनों के लिए ‘आश्रयस्थल’ में वृद्धि
2.आधरभूत सुविधओं जैसे शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और सफाई का प्रबंध आदि को उपलब्ध करवाना।
3.महिलाओं की ‘मूलभूत सेवाओं’ तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुँच में सुधार
4. उर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्र को उन्नत बनाना।
5. वायु प्रदूषण को कम करना।